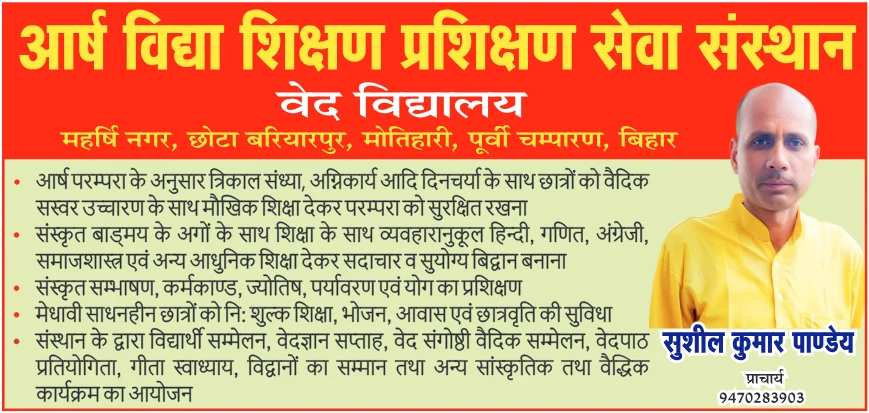@राजीव थेपड़ा
प्रेम की बाबत ऐसा कोई आदर्श-वादर्श मेरे जेहन में नहीं…मेरे लिए प्रेम एक जैविक इच्छा भी है और अपने प्रेम पात्र के लिए नैसर्गिक देह-ईच्छा भी…। हम इसे पवित्र-अपवित्र की संकीर्णताओं में बांध कर इसकी मासूम भावनाओं तक को कलुषित कर देते हैं। अपने विस्तृत विस्तार में यह ब्रह्मांड मात्र को ख़ुद में समेट लेने की इच्छा है।…तो, अपने तृण-रूप में अपने प्रिय-पात्र को स्वयं में समाहित कर लेने की व्याकुलता भी…! प्रेम के ये सब रूप हमारे जीवन के आधार हैं…! इसमें कुछ पाक या नापाक वाली कोई बात ही नहीं…! ये ढकोसले हमारी फ़िज़ूल की बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं हैं, जिसमें दरअसल कोई सार ही नहीं…! मगर, हम इसे अपनी विद्वता समझने का दम्भ पाले रहते हैं…!!
क्या है कि न जाने किन मीमांसाओं के आधार पर या कि किन शास्त्रों के आधार पर पवित्रता नामक एक शब्द प्रेम के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि प्रेम की जैविकता, उसकी नैसर्गिकता, पवित्रता नामक एक शब्द के इर्द-गिर्द गूंथ दी गयी है और इससे प्रेम का वह व्यापक स्वरूप ही खो गया है, जो एक सामान्य मनुष्य में प्राकृतिक रूप से व्याप्त होता है ! सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि इस प्रेम की कुछ नैसर्गिक आवश्यकताओं, जैविक इच्छाओं ; यानी शारीरिक आवश्यकताओं को कुंद कर लेने पर जोर दिखाई देता है !
आध्यात्मिक के क्षेत्र में प्रेम को चाहे जिस किसी दृष्टि से देखा जाये, लेकिन सामान्य मनुष्यता के क्षेत्र में प्रेम उसी प्रकार परिभाषित नहीं किया जा सकता। सामान्य जीवन में प्रेम का परिपूरक कुछ और हो ही नहीं सकता और वह अंततः कहीं ना कहीं थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, किन्तु दैहिक आवश्यकताओं पर जाकर रुक जाता है। यद्यपि, यह भी सच है कि केवल और केवल दैहिक इच्छाएं ही किसी भी प्रेम का लक्ष्य नहीं होतीं। प्रायः प्रेम में प्रमुखतः आपसी साहचार्य ही ध्वनित होता है और जहां ऐसा नहीं है, वहां प्रेम को प्रेम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, प्रेम केवल दैहिक इच्छाओं की पूर्ति भर नहीं है, किन्तु साथ ही प्रेम कोई दैविक या आध्यात्मिक प्रक्रिया भर भी नहीं है। प्रेम एक प्राकृतिक अवस्था है। इसमें हर कोई डूबना चाहता है और वह डूबना केवल इसलिए होता है कि प्रेम का जो रस है, प्रेम का जो सत्व है, प्रेम का जो सार है, वह एक-दूसरे से जुड़ाव का भाव है। क्योंकि, सामान्यतः प्रेम में दूसरे की इच्छा भी अपनी इच्छा के समान ही सर्वोपरि होती है। इससे आगे कहूं, तो जो जितना ज्यादा प्रेम में डूबते हैं, उनके लिए सामनेवाले की इच्छा अपनी इच्छा से ज्यादा सर्वोपरि बन जाती है।
इसलिए यह तो तय है कि प्रेम केवल दैहिक इच्छा भर नहीं है। यद्यपि, संसार में ऐसा भी होता है और यह भी अपनी-अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी में कम और किसी में ज्यादा के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ज्यादा दैहिक इच्छा रखनेवाला कम प्रेम करता हो और कम दैहिक इच्छावाला ज्यादा प्रेम करता हो। इन दोनों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं ढूंढी जा सकती और ना ही ऐसी कोई तुलना की जा सकती है। कोई जोड़ा बहुत ज्यादा दैहिक संसर्ग में डूब सकता है, तो कोई जोड़ा कम भी। कुछ भी होना सम्भव है। लेकिन, प्रेम को दैहिक इच्छाओं के इर्द-गिर्द, उसी के अनुसार परिभाषित करने की हमारी जो जिद है। हमारे शास्त्रों की जो जिद है या उनकी व्याख्या करते हुए अन्य लोगों की उससे भी ज्यादा जो जिद है, उससे प्रेम करनेवाले सामान्य मनुष्य अपने आप को एक तरह से अपराधी मानने लगते हैं ! क्योंकि, वहां पर दैहिक इच्छाओं को वर्जित किया जाता है और ये बातें समस्त धर्मों में व्याप्त हैं।
…और, यहीं पर धर्म और सामान्य जीवन का एक तरह का झगड़ा सामने आता है। सामान्य जीवन में प्रेम को हम किसी और रूप में देखते हैं। किन्तु, धार्मिक व्याख्या में प्रेम के उस रूप को एक तरह से प्रतिबंधित घोषित किया जाता है और ब्रह्मचर्य की महिमा बखान करते हुए दैहिक संसर्ग को तुच्छ समझा जाता है और ऐसा बताया जाता है। हो सकता है कि शास्त्रों में इसका बिलकुल वही अर्थ ना हो ; जैसा कि इसकी व्याख्या करनेवाले बताते हैं। किन्तु आम जीवन में तो आध्यात्मिक क्षेत्र के धार्मिक लोग इसे इसी प्रकार परिभाषित करते हैं और ऐसे में प्रेम के साथ ब्रह्मचर्य, शुचिता, पवित्रता यह सारी बातें आपस में इस प्रकार गड्डमगड्ड हो जाते हैं कि हर मनुष्य, नर – नारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका प्रेम एक आपराधिक कृत्य तो नहीं है ?? यहीं पर हम प्रेम की को गलत तरीके से देखने लगते हैं ! क्योंकि, हर किसी को यह लगता है कि उन्होंने दैहिक संसर्ग कर लिया, तो वह उनके प्रेम की शुचिता या पवित्रता भंग हो गयी !!
इस प्रकार बरसों से हम कुछ ऐसी बातों को, ऐसी परिभाषाओं को, ऐसी व्याख्याओं को अपने जीवन में ढोये जा रहे हैं या उसका गलत निरूपण किया जा रहे हैं। इसके चलते सामान्य जीवन जी रहे लोगों के लिए प्रेम एक अजीबोगरीब वितृष्णा बन गया है और इसीलिए यह एक छुपा-छुपी का खेल भी हो गया है। हजारों साल से, जब से हम लिखित इतिहास देख रहे हैं, तब से हम लगातार यही पाते हैं कि प्रेम को छिपे ढंग से किया जाता है। इसे छुपाया जाता है और प्रेम करनेवाले लोग छुपने की जगह ढूंढते रहते हैं ! क्योंकि, उनकी आपसी बातचीत को भी समाज ऐसे ढंग से देखता है कि प्रेम से बातचीत करनेवाले लोग भी अपने आप में लज्जित होते रहते हैं और कोई किसी को आलिंगनबद्ध देख ले, तब तो समझो कि तांडव मच जायेगा !!
प्रेम की उपरोक्त दृष्टियां प्रेम के स्वरूप पर, प्रेम के वास्तविक स्वरूप पर कुठाराघात करती हैं ! इसे समझा जाना चाहिए। इसे वास्तविक अर्थो में समझा जाना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी जीव एकांतसेवी नहीं होता ! सभी के समाज होते हैं, कबीले होते हैं। इस प्रकार मनुष्य नामक जीव का भी समाज है। परिवार है और इसके बगैर कोई जी ही नहीं सकता। इसलिए कृपया प्रेम में आध्यात्मिकता ना घुमाया ! सामान्य जीवन एक अलग प्रक्रिया है। आध्यात्मिक जीवन इससे उलट प्रक्रिया है। हालांकि, कहीं-कहीं इन दोनों में सामंजस्य भी पाया जाता है। लेकिन, ऐसा भी विरले ही देखा जाता है।…तो, कृपया हम इसे सहज ढंग से लें। प्रेम को सहजतापूर्वक ग्रहण करें। इसे हर एक की इच्छा के रूप में ग्रहण करें और किसी पर अनावश्यक प्रतिबंध न डालें । किसी विषय पर व्यर्थ की वर्जना न थोपें, यही अच्छा है।
इसी बात का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हम में से हर बड़ा या छोटा, मतलब बालक हो या व्यस्क या वृद्ध ! हर कोई अपने जीवन में किसी का प्रेम चाहता है । किसी का अपने प्रति भाव चाहता है। लेकिन वही व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के उनी भावों से घृणा करता है! ये एक तरह के परिहास ही तो हैं, जो कदम-कदम पर हमें तरह-तरह के झंझटों में डालते हैं! यानी इस प्रकार की झंझट हम स्वयं ही तो पैदा करते हैं ! काश…हम अपनी इच्छाओं की भांति दूसरे की भी उन्हीं इच्छाओं को समझ पाने में सक्षम हों, तो सम्भव है कि हम प्रेम के उस उदात्त स्वरूप को सहजता से अपने मन में वह स्थान दे पायेंगे, जिसके आकांक्षी हम स्वयं हैं और सदा से हैं और तभी प्रेम को वैसा सम्मान मिल पायेगा, जिसका अधिकारी वह है और उसी प्रकार समस्त प्रेम करनेवाले भी इस सम्मान के अधिकारी हैं, जिसे हम अपने जीवन में अभी तक अपेक्षित स्थान ही नहीं दे पाये हैं !
कुल मिला कर प्रेम के प्रति हमारे वर्तमान भाव में थोड़ी बदलाहट, थोड़ी-सी सारगर्भिता, थोड़ी सुचिंता, थोड़ा-सा सम्यक भाव चाहिए, जिससे हम अपने प्रिय पात्र के प्रति अपने प्रेम का प्रकटीकरण उचित भावों द्वारा कर सकें। इस प्रकार स्वयं अपना प्रकटीकरण भी बिना किसी सकुचाहट, बिना किसी झिझक, बिना किसी लज्जा के भाव के साथ कर सकें ! इसी में प्रेम नामक भाव का वास्तविक सम्मान है। इसी में मनुष्यता नामक हमारी सभ्यता का भी सम्मान है।