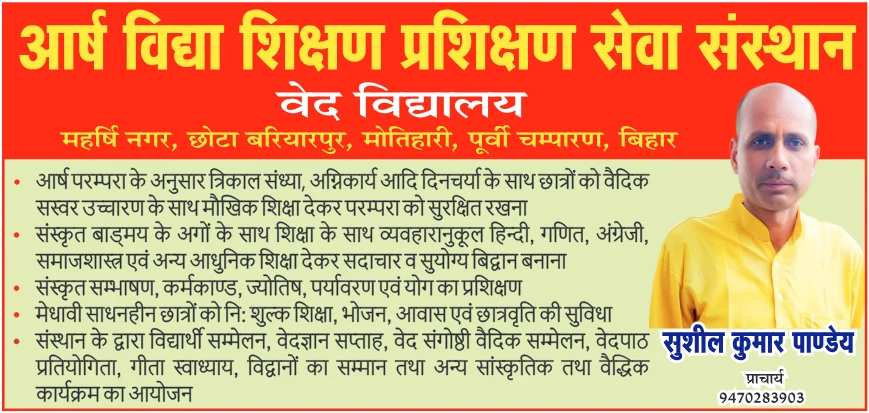राजीव थेपड़ा
हम क्या बचा सकते हैं…और क्या मिटा सकते हैं… यह निर्भर सिर्फ़ एक ही बात पर करता है कि हम आख़िर चाहते क्या हैं…हम सब के सब चाहते हैं…पढ़-लिख कर अपने लिए एक अदद नौकरी या कोई भी काम, जो हमारी जिन्दगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त धन मुहैया करा सके। हम अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें तथा शादी करके एक-दो बच्चे पैदा करके चैन से जीवन-यापन कर सकें।
मगर यहां भी मैंने कुछ झूठ ही कह दिया है, क्योंकि अब परिवार का भरण-पोषण करना भी हमारी जिम्मेवारी कहां रही। मां-बाप का काम तो अब बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करना और उन्हें काम-धंधे पर लगा कर अपनी राह पकड़ना है….बच्चों से अपने लिए कोई अपेक्षा करना थोड़ी ना है….! वे मरे या जियें बच्चों की बला से…!
खैर… यह तो विषयांतर हो गया। मुद्दा यह है कि हम जिन्दगी में क्या चुनते हैं और उसके केन्द्र में क्या है…!! और उत्तर भी बिलकुल साफ़ है कि सिर्फ़-व-सिर्फ़ अपना परिवार और उसका हित चुनते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि हम सबकी जिन्दगी में समाज कुछ नहीं…और उसकी उपादेयता शायद शादी-ब्याह तथा कुछेक अन्य अवसरों पर रस्म अदायगी भर पूरी के लिए है…यानी संक्षेप में यह भी कि समाज होते हुए भी हमारे रोजमर्रा के जीवन से लगभग नदारद ही है…! और, कुछेक अवसरों पर वह हमारे जीवन में अवांछित या वांछित रूप से टपक पड़ता है….! समाज की जरूरतें हमारी जरूरतें नहीं हैं…… और हमारी जरूरतें, समाज की नहीं….!!
अब इतने सारे लोग धरती पर जन्म ले ही रहे हैं…और वे भी हमारे आस-पास ही….तो कुछ-ना-कुछ तो बनेगा ही…! समाज ना सही…. कुछ और सही….और उसका कुछ-ना-कुछ तो होगा ही….यह ना सही….कुछ और सही…! तो समाज यथार्थ होते हुए भी दरअसल विलुप्त ही होता है…. ! जिसे अपनी जरूरत से ही हम अपने पास शरीक करते हैं और जरूरत ना होने पर दूध में मक्खी की तरह बाहर….तो, जाहिर है जब हम सिर्फ़-व-सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं, तो हम किसी को भी रौंद कर बस आगे बढ़ जाना चाहते हैं…! इस प्रकार सब ही तो एक-दूसरे को रौंदने के कार्यक्रम में शरीक हैं…और, जब ऐसा ही है, तो यह कैसे हो सकता है भला कि इक और तो हम जिन्दगी में आगे बढ़ने की होड़ में सबको धक्का देकर आगे बढ़ना चाहें और दूसरी ओर यह उम्मीद भी करें कि दूसरा हमारा भला चाहे….!!
ऐसी स्थिति में हम…हमारा काम…और हमारी नौकरी ही हमारा एक-मात्र स्वार्थ…एक-मात्र लक्ष्य…एक-मात्र…एक-मात्र अनिवार्यता हो जाता है…वह हमारी देह की चमड़ी की भांति हो जाता है, जिसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता…फिर चाहे जमीर जाये…चाहे ईमान…चाहे खुद्दारी….चाहे अपने व्यक्तित्व की सारी निजता…..!! हां, इतना अवश्य है कि कहीं…कभी सरेआम हमारी इज्ज़त ना चली जाये…..!! मगर, ऐसा भी कैसे हो सकता है कि एक ओर तो हम सबकी इज्ज़त उछालते चलें, दूसरी और यह भी चाहें कि हमारी इज्ज़त ढकी ही रहे। सो, देर-अबेर हमारी भी इज्ज़त उतर कर ही रहती है…!
दरअसल, दुनिया के सारे कर्म देने के लेने हैं….और, यह सारी जिन्दगी गुजार देने के बाद भी हम नहीं समझ नहीं पाते। यह भी बड़ा अद्भुत ही है ना कि दुनिया का सबसे विवेकशील प्राणी और प्राणी-जगत में अपने-आप सर्वश्रेष्ठ समझनेवाला मनुष्य जिन्दगी का ज़रा-सा भी पहाड़ा नहीं जानता…और जिन्दगी-भर सबके साथ मिल कर जीने के बजाय सबसे लड़ने में ही बिता देता है और सदा अंत में यह सोचता है कि हाय यह जिन्दगी तो यूं ही चली गयी…! कुछ कर भी ना पाये…..!! अब यह कुछ करना क्या होता है भाई….?? जब हर वक्त अपने पेट की भूख…अपने तन के कपड़े…अपने ऊपर इक छत के जुगाड़ की कामना भर में पागल हो रहे…और पागलों की तरह ही मर गये, तो यह कुछ करना भला क्या हुआ होता…??
जिन्दगी क्या है…? और, इसका मतलब क्या…? सबके साथ मिल कर जीने में अगर जीने का आनन्द है, तो यह आपाधापी…. यह काॅम्पीटिशन की भावना…. यह आगे बढ़ने की साजिश-पूर्ण कोशिशें…. यह कपट… यह धूर्तता… यह बेईमानी… यह छल-कपट….यह लालच… यह धन की अंतहीन….असीम चाहत….इन सबको तो हर हाल में त्यागना ही होगा ना….!!
जीने के लिए खाना यानी भोजन पहली और आखिरी जरूरत है।…और, इस जरूरत को पूरा करने के लिए धरती के पास पर्याप्त साधन और जगह है, मगर हमारी जरूरतें भी तो सुभान-अल्लाह किस-किस किस्म की हैं आज…!! फेहरिस्त सुनाऊं क्या…?? तो जब हमारी जरूरतों का यह हाल है…तो, हमारा हाल भला क्या होगा…? हमारी जरूरतों की तुलना में उनको प्राप्त करने के साधनों को कई गुना अधिक कर दें, तो हमारा वास्तविक हल निकल आये !!